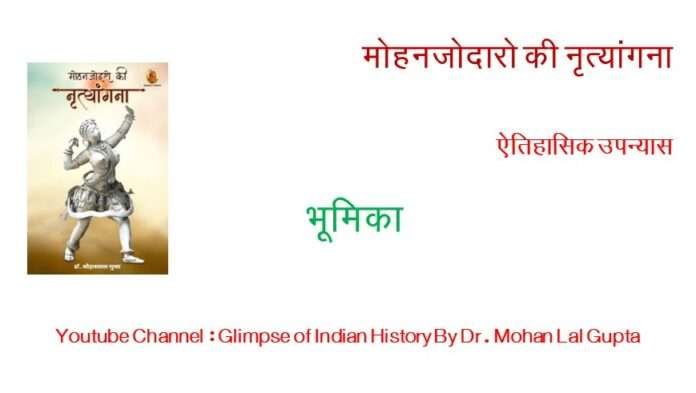मोहनजोदारो की नृत्यांगना भारत की दस हजार साल पुरानी सभ्यता पर लिखा गया एक उपन्यास है। इस उपन्यास में आधारभूत सामग्री के रूप में उस काल का वैदिक साहित्य एवं सैंन्धव पुरातत्व काम में लिया गया है।
शरीर रचना शास्त्र (Racical Anthropology) की दृष्टि से भारत भूमि पर निवास करने वाली आदिम जातियों के छः समुदाय- नीग्रेटो, प्रोटो-आस्ट्रेलायड, मंगोलायड, भूमध्यसागरीय द्रविड़, पश्चिमी बे्रचीसेफल तथा नोर्डिक बताये गये हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों हड़प्पा, मोहेन-जो-दड़ो और चहून्दड़ो से प्रोटो-आस्ट्रेलायड, भूमध्यसागरीय द्रविड़, मंगोलायड तथा अल्पाइन जाति के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं।
जबकि भारतभूमि पर आज निवास करने वाले मानव समुदाय में शरीर रचना शास्त्र की दृष्टि से मुख्यतः चार जनसमुदाय उपस्थित हैं- आर्य, द्राविड़, निषाद और किरात।
यह भी माना जाता है कि नीग्रेटो, प्रोटो-आस्ट्रेलायड, मंगोलायड, भूमध्यसागरीय द्रविड़, पश्चिमी बे्रचीसेफल तथा नोर्डिक आदिम समुदायों से द्राविड़, निषाद और किरात जनजातियों का उद्भव हुआ। इसका अर्थ है कि आर्य जनसमुदाय भारत के आदिम जनसमूह से अनुपस्थित है। उन्हें बाद में किसी अन्य प्रदेश से भारत भूमि में आना बताया जाता है।
आर्य, द्राविड़, निषाद और किरात जनसमुदाय कितने समय से भारत भूमि में निवास करते आये हैं, इस सम्बंध में निर्विवाद रूप से कहा जाना संभव नहीं है। अब तक उपलब्ध समस्त ऐतिहासिक, भाषाशास्त्रिक, पुरातात्त्विक और पौराणिक साक्ष्यों का उपयोग करके भी इन जनसमुदायों के भारत में निवास आरंभ करने की वास्तविक तिथियों का पता नहीं लगाया जा सका है। आज आर्य जनसमुदाय भारत भूमि पर निवास करने वाला सबसे बड़ा जनसमुदाय है।
आर्यों के सम्बन्ध में जहाँ कुछ विद्वानों का मत है कि वे किसी अन्य प्रदेश से भारत में आये वहीं बहुत से विद्वानों का मत है कि आर्य जनसमुदाय का उद्भव भारत भूमि पर ही हुआ तथा वे आदिकाल से भारतभूमि पर ही रहते आये हैं। दोनों ही मान्यताओं के पक्ष में प्रबल तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं।
यदि आर्य जाति के प्रागैतिहासिक अस्थिपंजर प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जहाँ अन्यान्य प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में शवाधान की परम्परा थी वहीं आर्य जाति में शवदाह की परम्परा थी।
भारत के पश्चिमोत्तर भाग से प्राप्त सिंधुघाटी सभ्यता को आज सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष माना जाता है । इससे पूर्व की बस्तियाँ आदिमयुगीन मानी जाती हैं। जिनमें विकसित सभ्यता का अभाव है। पुरातात्विक अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं से प्राचीन होते हुए भी सिंधु सभ्यता तृतीय कांस्य कालीन तथा अत्यंत विकसित सभ्यता थी।
भूमध्यसागरीय द्राविड़ जनसमुदाय इस सभ्यता का जनक माना जाता है। ब्राहुई भाषा और उनके बोलने वालों के बलूचिस्तान में द्वीपवत् ठहरे हुए मिलने से इस मत का समर्थन किया गया है और कल्पना की गयी है कि बाद में यह समुदाय सिंधु घाटी से समुद्र के किनारे होकर सुदूर दक्षिण की ओर चला गया। जहाँ वह आज भी विद्यमान है।
चूंकि सिंधु सभ्यता आज अपने स्थान पर उपस्थित नही है और उस क्षेत्र में आर्य जाति निवास करती है इसलिये पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन आर्यों पर यह दोष आरोपित किया है कि आर्य असभ्य, बर्बर और लड़ाकू थे, उन्होंने सिंधु सभ्यता का विध्वंस कर दिया।
इस उपन्यास का उद्देश्य सैंधवों और आर्यों के मध्य रहे सम्बन्धों तथा उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना है जिनमें सैंधव और आर्य सभ्यतायें एक दूसरे के साथ रहते हुए संघर्ष और समन्वयन के प्रयास कर रही होंगी।
एक तरफ तो पश्चिमी विद्वान आर्यों को असभ्य, बर्बर और लड़ाकू बता रहे हैं तो दूसरी तरफ वेदों की उपस्थिति बता रही है कि सैंधव सभ्यता के समकालिक आर्यों में शुभ और अशुभ कर्मों का पूरा विवेक था जिसके कारण आर्य असभ्य और बर्बर नहीं कहे जा सकते। आर्यों ने वेदों में स्थान-स्थान पर अपने जिन शत्रुओं का उल्लेख किया है, उन्हें अशुभ कर्मों को करने वाला बताया है।
हम यह भी देखते हैं कि आर्यों ने आगे चलकर सैंधवों की बहुत सी मान्यताओं और परम्पराओं को स्वीकार कर लिया। जिनमें नाग पूजा, पशु-पक्षियों की पूजा, लिंग और योनि की पूजा, मूर्तिपूजा तथा बलिप्रथा आदि प्रमुख हैं। उनमें से बहुत सी आज तक प्रचलित हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि आर्यों ने सैंधवों को नष्ट नहीं किया।
अपितु ये दोनों सभ्यतायें लम्बे समय तक साथ-साथ रहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो सैंधवों की बहुत सी बातों को आर्यों ने धार्मिक विश्वास के रूप में नहीं अपनाया होता। इन्हीं रीति-रिवाज़ों के आधार पर कुछ विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सिंधु सभ्यता के जनक और आर्य एक ही थे, अलग-अलग नहीं थे।
अब तक जो भी ऐतिहासिक, भाषाशास्त्रिक, पुरातात्त्विक और पौराणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे सिंधु सभ्यता वासियों तथा ऋग्वैदिक आर्यों के सम्बंध में यही धारणा बनती है कि सैंधव सभ्यता के निर्माता आर्यों से भिन्न तथा पूर्ववर्ती थे। सैंधव सभ्यता नगरीय थी जबकि आर्य ‘चरवाहों के जन’ थे।
सैंधव सभ्यता मूर्तिपूजक थी जबकि आर्य अमूत्र्त देवताओं के उपासक थे। सैंधव देव-पूजन में जल को अधिक महत्व देते थे जबकि आर्य अग्नि पूजक थे। सैंधव सभ्यता अश्व से अपरिचित थी जबकि आर्य अश्वपालक थे। सैंधव सभ्यता शांतिप्रिय थी जबकि आर्य युद्ध प्रेमी थे। सैंधव सभ्यता लिपि का प्रयोग कर अपने लेख मुद्राओं, आभूषणों, बर्तनों और अन्य सामग्री पर अंकित कर रही थी जबकि आर्य ज्ञान को स्मृति के माध्यम से सुरक्षित रख रहे थे।
सैंधव सभ्यता के प्रसार क्षेत्र के केन्द्र में महानद सिंधु था जबकि वैदिक सभ्यता के भूगोल में महानदी सरस्वती केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन कर रही थी। सैंधव सभ्यता चित्रित मृद्भाण्डों वाली सभ्यता है जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की बस्तियों से धूसर मृदभाण्ड प्राप्त हुए हैं। सिधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र से जो भी आर्य सामग्री यथा मृदभाण्ड एवं यज्ञकुण्ड प्राप्त हुए हैं, वे परवर्ती काल के हैं।
सिंधु सभ्यता की बस्तियाँ बलूचिस्तान, उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ तथा पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों से मिली हैं। जबकि वेदों में जिन नदियों का वर्णन आया है उनसे पता चलता है कि ऋग्वेद की रचना अफगानिस्तान और पंजाब तक के विस्तृत प्रदेश में हुई। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुभा, सुवास्तु, गोमती एवं क्रुमु तथा पंजाब की शतुद्रि, विपाशा, परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता नामक नदियों का उल्लेख कई बार हुआ है।
सिंधु तथा सरस्वती का उल्लेख भी पर्याप्त बार हुआ है साथ ही गंगा-यमुना का उल्लेख भी आया है। स्पष्ट है कि वेदों की रचना के प्रारंभिक काल में आर्य हिन्दुकुश पर्वत से गंगा तक फैले हुए थे। पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि इसके बाद वैदिक जनों का प्रसार पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण दिशाओं की ओर हुआ।
‘आर्य-जन’ एवं ‘सिंधु-सभ्यता’ के प्रसार क्षेत्र सटे हुए थे तथा ये दोनों सभ्यतायें समकालीन थीं। दोनों सभ्यताओं के रहन-सहन एवं चिंतन में काफी अन्तर था। अतः स्वाभाविक ही था कि दोनों सभ्यताओं में संघर्ष होता। इस संघर्ष का परिणाम भी स्वाभाविक रूप से दो या तीन रूप ले सकता था-(1) दोनों सभ्यताओं में से कम से कम कोई एक सभ्यता नष्ट हो जाये। (2) दोनों सभ्यताओं में से कम से कम कोई एक सभ्यता अपना स्थान परिवर्तित कर ले अथवा (3) दोनों सभ्यताओं में समन्वय स्थापित हो जाये।
प्रकृति का नियम है कि संघर्ष और समन्वयन साथ-साथ चलते हैं। यही आर्यों और सैंधवों के बीच भी हुआ होगा। इसी कारण आर्यों ने सैंधवों को अपने से हीन समझते हुए भी उनकी बहुत सी बातें अपना लीं जो आज भी आर्यों में प्रचलित हैं। यह अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है कि संघर्ष में सक्षम नहीं होने के कारण सैंधव अपने क्षेत्र से धीरे-धीरे पलायन कर गये और उनके क्षेत्रों पर आर्यों ने अपनी बस्तियाँ बसा लीं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यों ने उन्हें बर्बरता से नष्ट किया।
आर्यों ने वेदों में स्थान-स्थान पर अपने शत्रुओं का उल्लेख किया है, जिससे पश्चिमी विद्वानों ने उन्हें बर्बर, लड़ाकू और आक्रांता मान लिया है। अनुमान होता है कि आर्यों का संघर्ष बहुकोणीय था। एक तरफ वे पणियों, असुरों और दस्युओं से युद्ध कर रहे थे तो दूसरी ओर उनमें परस्पर संघर्ष भी था। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में यह संघर्ष देवासुर संग्राम तथा देवताओं के संघर्ष के रूप में वर्णित है।
सैंधव सभ्यता कितनी पुरानी थी तथा कब आरंभ होकर अपने चरम पर पहुँची इस सम्बंध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। इस कार्य में रेडियो कार्बन विधि से किया गया तिथि निर्धारण भी अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है। जीवधारियों में कार्बन-14 ग्रहण करने की दर विश्व के सभी क्षेत्रों में सदैव एक सी नहीं रहती।
इसी प्रकार वैदिक सभ्यता कब आरंभ होकर कब अपने चरम पर पहुँची, कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सका है। ऋग्वेद को एक हजार ईसा पूर्व से लेकर पच्चीस हजार ईसा पूर्व तक पुराना माना गया है। सभी विद्वान अपने-अपने समर्थन में प्रबल मत देते हैं दूसरे विद्वान द्वारा प्रस्तुत मत का तो खण्डन करते हैं किंतु अपने मत के समर्थन में दूसरे विद्वानों द्वारा व्यक्त शंका का समाधान नहीं कर पाते हैं।
काल सम्बन्धी प्रश्नों के समुचित उत्तर दे पाना आज भले ही संभव न हो पा रहा हो किंतु यह निश्चित है कि आज से सहस्रों वर्ष पहले का मानव भी उच्च एवं विकसित संस्कृति से परिचित था। सैंधव सभ्यता तथा ऋग्वैदिक आर्य सभ्यता उस काल में महान सभ्यतायें थीं जिनके सम्बन्ध दूर-दूर तक की सभ्यताओं से थे तथा उनमें एक सम्पर्क भाषा भी थी। मेसोपोटामिया में सैंधव व्यापारियों की भाषा का अनुवाद करने के लिये दुभाषियों की भी व्यवस्था की गयी थी।
सिंधु सभ्यता का सम्बन्ध विश्व की तत्कालीन सभ्यताओं से रहा होगा, इसके कई प्रमाण मिलते हैं। ईरान के प्राचीन नगर सूसा तथा ईलम ईसा से 2500 वर्ष पहले भी अस्तित्व में थे। ये दजला-फरात नदियों के किनारे पर बसी मेसोपोटामिया सभ्यता के निकट स्थित हैं। यहाँ से सिंधु सभ्यता की मुहरें पाई गयी हैं। इसी प्रकार मेसोपोटामिया की कुछ मुहरें सिंधु स्थलों से भी प्राप्त हुई हैं। स्पष्ट है कि इन नगरों का सिंधु सभ्यता से सम्बन्ध था। मिश्र के एक पिरामिड से सैंधव गुरिया (माला में पिरोने की मणि) प्राप्त हुई है।
इसी प्रकार भारतीय आर्यों का सम्बन्ध भी विश्व की तत्कालीन सभ्यताओं से होने के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। पिरामिड शब्द संस्कृत के ‘परम़्$इदम्’ से साम्य रखता है। इन पिरामिडों का निर्माण फरोह राजाओं द्वारा करवाया गया। फरोह शब्द का साम्य संस्कृत शब्दों-‘परा़$रोह’ से है जिसका अर्थ ‘महानाविक’ होता है।
अनुमान होता है कि मिश्र सभ्यता के फरोह शासक भारतीय आर्य थे जो समुद्र के रास्ते मिश्र पहुँचे। पिरामिडों के निर्माण के बाद मिश्र में ‘हतशेषसुत’ नाम का राजा हुआ। जिसने अपनी राजधानी कर्नाक में विशाल पाषाण मूर्तियाँ, भवन और पिरामिड बनवाये। संस्कृत में हतशेषसुत का शाब्दिक अर्थ होता है- ‘मर जाने से शेष बचे मनुष्य का पुत्र’ अथवा ‘मरे हुए पुत्रों में से शेष बचा हुआ।’
इस काल में मिश्र का मुख्य देवता ‘रा’ अथवा ‘रे’ (सूर्य) है जो ‘रवि’ शब्द से साम्य रखता है। हम्मूराबी की विधि संहिता एक बेलनाकार पत्थर पर खुदी है जिसमें सम्राट को सूर्य देवता से नियमों को प्राप्त कते हुए दिखाया गया है। ऋग्वेद में सूर्योपासना से सम्बंधित अनेक ऋचायें मिलती हैं। मिश्र के एक पिरामिड से मिट्टी की एक मुद्रा प्राप्त हुई है।
यह लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है। इस मुद्रा पर किसी वृक्ष की एक शाखा अंकित है जिसपर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उसे देख रहा है। मुण्डकोपनिषद में इस रूपक का उल्लेख है जिसके अनुसार इनमे से पहला पक्षी जीव है जो कर्मफल का भोग करता है तथा दूसरा पक्षी ब्रह्म है जो इस भोग का साक्षी है।
एशिया माइनर (वर्तमान टर्की) में स्थित बोगाजकुई से एक शिलालख प्राप्त हुआ है जिसमें मितानी देवों- मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नासत्यौ (अश्विनी) के उल्लेख हैं। मितानी जाति भारतीय आर्यों की एक शाखा थी जो भारत से जाकर पश्चिम एशिया में बस गयीथी। इसी लिये इस अभिलेख में आर्य देवताओं का उल्लेख है।
ये देवता वैदिक युग से पूर्व के हैं तथा अविभाजित भारतीय एवं ईरानी आर्यों के सामूहिक देवता हैं। यह अभिलेख ईसा से एक हजार पाँच सौ वर्ष पुराना माना जाता है। अर्थात् इस समय से काफी पहले भी आर्य वहाँ निवास करते रहे होंगे। संभवतः ईसा से पाँच हजार साल पहले भी। बोगाजकुई अभिलेख में जिन देवों का उल्लेख है उनमें मित्र एवं वरूण के लिये ‘इलानि’ (त्रदेवाः) का प्रयोग हुआ है।
इस बहुवचन के प्रयोग से अनुवाद्य मूल में देवताद्वन्द्व की सूचना मिलती है। खत्ती (हित्तिति) शासक शब्बिलुल्यूमा और मितानी (मितन्नी) शासक मत्तिवाजा के बीच एक संधि करने के संदर्भ में ये देवता साक्षी के रूप में उल्लेखित किये गये हैं। संभवतः भारतीय अश्वपालक आर्यों की भी एक बस्ती यहाँ पर थी जिनका मुखिया मत्तिवाजा था, इसीलिये उन आर्यों में प्रचलित मित्र तथा वरुण आदि देवताओं को भी साक्षी के रूप में बुलाया गया था।
बाइबिल तथा इजराइल के इतिहास में सेनापति सिसेरा (शिशिर) की नाजरथ (नवशतरथ, अर्थात् लोहे के नौ सौ रथों वाली) सेना का उल्लेख होता है जो हेरोसेश हगोयम (हर्षस्थ यज्ञम्) नामक स्थान पर पड़ाव डाले हुए रही। इस सेनापति की हत्या यहूदियों ने धोखे से की। विश्व में लोहे का सर्वप्रथम उपयोग भारतीय आर्यों ने ही किया था।
इसी लिये अन्य सभ्यता वालों ने लोहे को आर्यों के नाम पर आयरन (आर्यन) कहकर पुकारा। विशाल लोहे के रथों वाली सेना भारत से ही वहाँ पहुँची थी जिनका पूर्वज ईस्वी पूर्व 1716 में एकोम (एकोअहम्) था। लगभग उसी काल का कांसे का बना एक तरकश ईरान में मिला है जिसपर वरुण, मित्र, इंद्र, पर्जन्य आदि वैदिक देवताओं से सम्बन्धित गाथा को व्यक्त किया गया है। वैदिक ऋषि च्यवन का जीवनवृत्तांत भी इस तूणीर पर उत्कीर्ण है।
आर्यों के परस्पर संघर्ष का विवरण देवों के संघर्ष के रूप में वर्णित है। इसी कारण वरुण ऋक् संहिता के महान् देवता हैं फिर भी उनकी पहचान विवादग्रस्त है। उनके लिये असुर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। वे ऋत अर्थात प्रकृति की व्यवस्था के रक्षक हैं, उन्हें ऊरानॉस, आकाश, रात्रिकालीन आकाश अथवा चन्द्रमा भी बताया गया है।
वरुण देवता ईरान में अहुरमज्दा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऋग्वेद में कहा गया है कि अस़ुर शक्ति से सम्पन्न होने के कारण वरुण कुपित होकर मनुष्यों का नाश कर सकता है (ऋग्वेद. 2 . 28 . 7) परन्तु ऋतवान् और घृतवृत होने के कारण वह पापियों के प्रति भी सहृदय हो जाता है और उन्हें क्षमा प्रदान कर देता है (ऋ. 7. 87 . 7)। व्रत पालन और यज्ञ कर्म से वह प्रसन्न रहता है (ऋ. 5 . 85 . 8)।
प्रसन्न होने पर वह सुख समृद्धि देता है (ऋ. 1 . 24 . 9)। ऋग्वेद का सातवाँ मण्डल वरुण स्तोत्रों से भरा पड़ा है। अथवर्ववेद के अनुसार मित्र को श्वेतवर्ण और वरुण को कृष्णवर्ण के पशु की बलि दी जाती है।
ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है- मैं पिता असुर (वरुण) का परित्याग कर रहा हूँ, यद्यपि उनके साथ मैं वर्षों तक अति सौहार्द्रभाव से रहा हूँ। अग्नि, वरुण और सोम को अब हट जाना चाहिये। प्रभुता दूसरे के पास जा रही है (ऋ. 10. 124)। इस उद्धरण से अनुमान होता है कि इन्द्र वरुण को अपदस्थ कर देवों का प्रमुख बना था।
वेद में एक ऋचा आती है जिसमें कहा गया है कि इन्द्र ने वरुण को देवत्व प्रदान किया। महाभारत के शल्य पर्व में उल्लेख है कि पूर्वकल्प में देवताओं ने जाकर वरुण से कहा- ‘इंद्र भय से हमारा त्राण करते रहते हैं। आप जल का अधिपत्य स्वीकार कीजिये ताकि आप भी हमारी रक्षा कर सकें। आपका निवास स्थान भी मकरालय में है।
वरुण ने देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार चतुर्थ ब्राह्मण के ‘सवनाम’ नामक पाँचवे काण्ड में उल्लेख है कि एक बार जब वरुण का अभिषक हो रहा था तब तब उसका तेज दूर चला गया। यज्ञ उससे हट गया। संभृत जलों का जो रस उसके अभिषेक में प्रयुक्त हुआ था उससे ही वरुण का तेज नष्ट हुआ। तब वरुण तेज प्राप्ति के लिये देवताओं के साथ संसर्पित हुआ। इस उल्लेख से भी अनुमान होता है कि इंद्र द्वारा अपदस्थ किये जाने के पश्चात् देवताओं ने वरुण को पुनः देवत्व प्रदान किया।
एक वैदिक आख्यायिका के अनुसार वरुण के प्रकोप से प्रजा जीर्ण-शीर्ण होने लगी और श्वांसमात्र को शेष रह गयी तब प्रजापति ने वरुणप्रघास नामक यज्ञ करके प्रजा की चिकित्सा की। प्रजा वरुण-पाश से मुक्त होकर निरोग और निर्मल हुई। ब्रह्मा द्वारा प्रजा को वरुण के पाश से मुक्त करवाने की स्मृति में ऋग्वैदिक काल में वर्षाकाल आरंभ होने पर ”वरुणप्रघास” का आयोजन किया जाता था। (चतुर्थ ब्राह्मण 2. 5 . 2 -2 . 6 . 4) वरुण की पुत्री ‘वारुणि’ अर्थात् सुरा और वरुण के पुत्र ‘बल’ ने असुरों की शक्ति बढ़ायी।
उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए इस उपन्यास में वरुण को असुरों के मित्र के रूप में वर्णित किया गया है जिसे वृत्रासुर बंदी बना लेता है। इंद्र वृत्रासुर का वध कर वरुण को मुक्त करवाते हैं। देखा जाये तो पूरे वैदिक वाङ्मय में इन्द्र की सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही है।
सिंधु सभ्यता के नगरों के जो नाम इस उपन्यास में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें सिंधु सभ्यता के निवासी किन नामों से जानते थे, अब ज्ञात नहीं है। इसलिये उपन्यास में उन नगरों को आज प्रचलित नामों से सम्बोधित किया गया है। मेसोपोटामिया से मिली मोहरों से मेलुह्ह, मगन तथा दिल्मुन नामक नगरों के नाम मिले हैं जो संभवतः सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे तथा मेसोपोटामिया के व्यापारी इन नगरों से व्यापारिक सामग्री आयात करते थे। अतः इन नामों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है।
पूर्वैतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हुए भी ‘मोहनजोदारो की नृत्यांगना’ इतिहास नहीं है, उपन्यास है जिसमें उपन्यासकार को कल्पना करने के लिये पूरी स्वतंत्रता उपलब्ध रहती है। इसी कारण ‘मोहनजोदारो की नृत्यांगना’ के समस्त पात्र तथा घटनायें काल्पनिक हैं। उपन्यास का वातावरण वही रखा गया है जिसका आभास सिंधु सभ्यता के नगरों की खुदाई से प्राप्त सामग्री तथा वैदिक वाङ्मय से होता है ताकि पाठक भारत भूमि पर सहस्रों वर्ष पूर्व पुष्पित-पल्लवित होने वाली दो महान् सभ्यताओं के वैभव से परिचय का आनंद उठा सकें। इस कार्य में लेखक को कितनी सफलता मिली है, इसका निर्णय तो सुधि पाठकों को ही करना है। शुभम्।
-डॉ. मोहनलाल गुप्ता