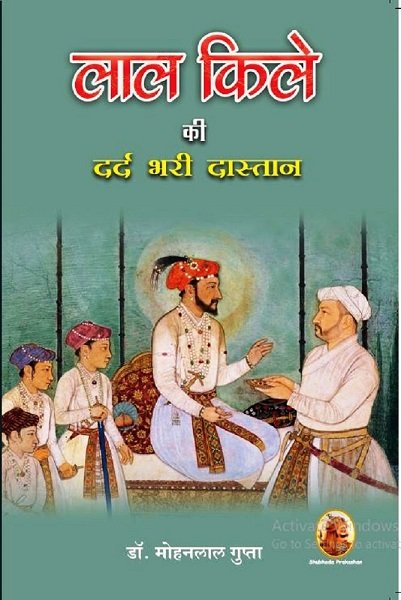लाल किले की कंगाली मुगलों के इतिहास की एक काली सच्चाई है जो शायद ही कभी इतिहास के पाठकों के समक्ष लाई गई है। इस कंगाली को देखकर लाल किले के साथ-साथ भारत माता भी आंसू बहा रही थी!
ईस्वी 1757 में अहमदशाह अब्दाली के अफगानिस्तान लौट जाने के बाद बादशाह आलमगीर मराठों के भय से अपने परिवार के साथ लाल किले से बाहर निकलकर जाटों की शरण में डीग भाग गया था तथा महाराजा सूरजमल की सेना के संरक्षण में वह फिर से लाल किले में प्रवेश पा सका था।
कहने को तो आलमगीर (द्वितीय) अब भी बादशाह था और दिल्ली के तख्त पर बैठा था किंतु सच्चाई यह थी कि दिल्ली तो दूर लाल किले पर भी उसका शासन नहीं चलता था।
आलमगीर (द्वितीय) के समय में लिखी गई पु़स्तक ‘तारीख-ए-आलमगीर सानी’ में बादशाह की दुर्दशा और कंगाली का भयावह चित्रण किया गया है। इसमें लिखा है कि बादशाह इतना निर्धन हो चुका था कि उसके पास जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने हेतु कोई सवारी नहीं बची थी। रिसाले के घोड़े बिक चुके थे और तीन वर्ष से सैनिकों को वेतन नहीं मिला था।
लाल किले की कंगाली का हाल यह था कि महल के सब भण्डार खाली पड़े थे। पैदलों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। बादशाह के खास हाथी और घोड़ों को भी दाना नहीं मिलता था। जब बादशाह बाहर जाता था तो उसके साथ कोई नहीं जाया करता था।
पूरे आलेख के लिए देखें यह वी-ब्लॉग-
जब आलमगीर ने अपना जन्मदिन मनाया तो उसकी विपन्न अवस्था का भयंकर चित्र लोगों के सामने उपस्थित हुआ। रत्न-जटिज मयूरासन के स्थान पर एक काष्ठ-निर्मित चौकी थी जिस पर हीरे-जवाहरात के चित्र बने हुए थे। लाल किले की कंगाली का इससे बुरा चित्रण और क्या हो सकता था!
दीवाने खास में इने-गुने नौकर थे। न कोई अमीर था और न कोई राजा। बादशाह स्वयं मुगलों के विलीन वैभव का एक वीभत्स खण्डहर प्रतीत होता था।लाल किले की कंगाली ने मुगल शहजादियों का बुरा हाल किया। एक बार कई दिन की निरंतर भूख से पीड़ित होकर शहजादियां परदा तोड़कर शहर में जाने लगीं जिन्हें बड़ी कठिनाई से रोका गया।
जब स्वयं बादशाह तथा उसके हरम की यह हालत थी तो जनता की दुर्दशा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था। दिल्ली की जनता को पूरी तरह उसके दुर्भाग्य के हवाले कर दिया गया था। अफगान, रूहेला, जाट और मराठा सेनाएं मुगलों की परम्परागत शत्रु होने के कारण दिल्ली को लूट रही थीं, नष्ट कर रहे थीं और उसका बचा-खुचा जीवन धूल में मिला रही थीं।
इस काल की दिल्ली संभवतः थी ही इस योग्य। जब किसी देश के शासक अपने शत्रुओं से लड़ना छोड़कर और अपनी प्रजा का हित-चिंतन करना त्यागकर अपनी स्वार्थपूर्ति में लग जाते हैं अथवा रंगरेलियों में डूब जाते हैं, तब उनकी राजधानी, उनकी प्रजा और उनके राज्य का यही हाल होता है जो इस समय दिल्ली का हो रहा था। इस समय की दिल्ली पाण्डवों वाली दिल्ली नहीं थी, यह दिल्ली तोमरों वाली दिल्ली नहीं थी, यह दिल्ली चौहानों वाली दिल्ली भी नहीं थी। यह दिल्ली खलीफाओं की सेनाओं द्वारा सैंकड़ों साल तक लूटी गई, नौंची गई और पददलित की गई दिल्ली थी जो मंगोलों, बलोचों, ईरानियों, अफगानियों एवं तुर्कों के रूप में भारत आती रही थीं।
यह दिल्ली चंगेज खाँ और तैमूर लंग के रक्त मिश्रण से उत्पन्न बाबर की दिल्ली थी जिसके वंशज विगत दो सालों से मुगल बादशाहों के रूप में भारत का खून चूस रहे थे। इस समय की दिल्ली वह दिल्ली थी जिसने तेरहवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर अठारहवीं शताब्दी ईस्वी तक के पांच सौ सालों में भारत की जनता का रक्त पीकर अपने खजाने को समृद्ध किया था। दिल्ली का दुर्भाग्य यह था कि वह इस खजाने को सहेज कर नहीं रख सकी थी।
लाल किलों का सारा खजाना नादिरशाह एवं अदमदशाह अब्दाली जैसे दुर्दांत लुटेरे ले जा चुके थे औद दिल्ली पूरी तरह श्रीहीन होकर, धूल में लोट रही थी।
जो दिल्ली पाण्डवों से लेकर तोमरों और चौहानों तक के काल में भारत के करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए विख्यात थी, आज उसी दिल्ली में मौत और भूख का नंगा नाच हो रहा था। इन दिनों प्रकृति भी जैसे दिल्ली से नाराज हो गई थी।
दिल्ली से कुछ ही दूरी पर ब्रज को हैजे से मुक्ति मिली ही थी कि दिल्ली में दिमागी बुखार की महामारी फैली। यह महामारी अभी थमी भी नहीं थी कि आंखों में संक्रमण का भयानक रोग फैल गया। एक के बाद एक करके आती महामारी से त्रस्त, भूखे-नंगे लोग अपने घरों में पड़े तड़पते रहे, उन्हें औषधि और अन्न का कण देना तो दूर, पानी की बूंद तक पिलाने वाला कोई नहीं था।
नवम्बर 1757 में दिल्ली में जोरों का भूकम्प आया जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में घर गिर गये और सैंकड़ों लोग मर गये। खाने की चीजें बहुत महंगी हो गईं और दवाइयां तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती थीं। शहर में लुटेरों और चोरों के झुण्ड आ बसे जो राहगीरों को दिन दहाड़े लूटते थे।
लुटने और लूटने के लिए दिल्ली के लोगों के तन पर पहने हुए कपड़ों, दो-चार सेर अनाज और एकाध समय की रोटियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सदियों से भारत की राजधानी रही दिल्ली, खण्डहरों और शवों की नगरी बनकर रह गई।
दिल्ली के चारों ओर खेत पसरे हुए थे किंतु किसानों की हिम्मत नहीं होती थी कि वे उनमें बीज डाल दें। बीज बो भी दिया और फसल पक भी गई तो किसानों के हाथ आने वाली नहीं थी। कौन जाने उसे मुगलों के सैनिक लूट कर ले जाएंगे, या रूहेलों के या फिर ईरान से आया हुआ नादिरशाह खा जाएगा अथवा अफगानिस्तान से आया हुआ अहमदशाह इस फसल को छीन लेगा, यह भी तो पता नहीं था। फसल बोएं भी तो किसके लिए!
फिर भी किसानों को जीना ही था, अपने बच्चों का पेट पालना ही था। इसलिए खेत इस काल में भी बोए जा रहे थे और देश के करोड़ों किसान केवल इस आशा पर जीवित थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन परमपिता परमात्मा आएगा और सबके दुःख दूर कर देगा!
हिंदुकुश पर्वत के इस तरफ बह रहीं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, गंगा तथा यमुना अब भी जल से भरी हुई थीं। भारत की गाएं अब भी दूध देती थीं, धरती अब भी धान देने को तैयार थी किंतु हिन्दूकुश पर्वत के उस पार से आए हिंसक लोगों ने भारत की नदियों, पशुओं और धरती माता की जो दुर्दशा की थी, उसी का यह परिणाम था कि इस काल की दिल्ली में किसी का पेट नहीं भरता था।
भारत की शस्य-श्यामला भूमि को भेड़िए और लक्कड़बग्घे रौंद रहे थे। लाचार भारत माता की आंखों से आंसुओं के स्थान पर रक्त के झरने बहते थे किंतु भारत माता की आंखें पौंछने वाला कोई नहीं था।
दिल्ली के दुखों का अंत अभी निकट नहीं था। अभी तो अहमदशाह अब्दाली को एक बार वापस आना था। जैसे-जैसे मराठे पंजाब में आगे बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे काबुल में बैठा हुआ अहमदशाह अब्दाली गुस्से से उबल रहा था। जब ईस्वी 1758 में मराठों द्वारा उसका पुत्र तिमूरशाह लाहौर से भगा दिया गया तो अहमदशाह अब्दाली के क्रोध का पार नहीं रहा किंतु इस समय उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह तत्काल भारत जाकर मराठों का दमन कर सके।
उसकी सेना दिल्ली एवं मथुरा के अभियान से कुछ माह पहले ही लौटी थी तथा उसके बहुत से सैनिक हैजे से मारे गए थे इसलिए सेना का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। जो सैनिक जीवित लौटकर आए थे उनके पास इतना धन हो गया था कि अब उन्हें जिंदगी में फिर कभी लड़ाई पर जाने की आवश्यकता ही नहीं रही थी।
अहमदशाह अब्दाली के सेनापति भी तुरंत फिर से भारत चल देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अब्दाली ने सही समय आने तक काबुल में ही रुकने का निर्णय लिया किंतु अब्दाली से पहले तो फिरंगियों के रूप में एक और बड़ी मुसीबत दिल्ली के लाल किले की ओर बढ़ी चली आ रही थी जो हमेशा-हमेशा के लिए दिल्ली का रंग और रूप बदल देने वाली थी!
-डॉ. मोहनलाल गुप्ता